
पाठ 1 पद (हम तौ एक एक करि जांनां) कबीरदास आरोह भाग 1 काव्य खंड (11th हिन्दी) || पाठ का सारांश एवं संपूर्ण अभ्यास (प्रश्न उत्तर)
पद 1.
हम तौ एक एक करि जांनां ।
दोइ कहैं तिनहीं कौं दोजग जिन नाहिंन पहिचांनां ।।
एकै पवन एक ही पानीं एकै जोति समांनां ।
एकै खाक गढ़े सब भांडै एकै कोहरा सांनां ।।
जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटै अगिनि न काटै कोई ।
सब घटि अंतरि तँही व्यापक धरै सरूपै सोई ।।
माया देखि के जगत लुभांनां काहे रे नर गरबांनां ।
निरभै भया कछू नहिं ब्यापै कहै कबीर दिवांनां ।।
पद के बारे में
'कबीर के पद' नामक इस पद में कबीरदास ने परमात्मा को एक बताया है। उन्होंने ईश्वर के एकमात्र स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया कि जिस प्रकार सभी के लिए समान हवा बहती है, समान जल प्रवाहित होता है और सभी जीव एक ही परम प्रकाश पुँज में समाहित हो जाते हैं। साथ ही, जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से समस्त प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने भी हम सभी की रचना की है। मनुष्य को माया के भ्रम में न पड़कर भयमुक्त भाव से उस परमेश्वर के ऐकेश्वर रूप को स्वीकार करना चाहिए।
कवि परिचय
कबीर
जन्मतिथि एवं स्थान― सन् 1398, वाराणसी' के पास 'लहरतारा' (उ.प्र.)
प्रमुख रचनाएँ― 'बीजक' जिसमें साखी, सबद एवं रमैनी संकलित हैं।
मृत्यु तिथि एवं स्थान― सन् 1518 में बस्ती के निकट मगहर में।
संक्षिप्त परिचय― कबीर भक्तिकाल की निर्गुण धारा (ज्ञानाश्रयी शाखा) के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ़ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे, 'बन पड़े तो सीधे-सीधे नहीं तो दरेरा देकर।' इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'वाणी का डिक्टेटर' कहा है।
कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसि कागद छुयो नहि कलम गहि नहि हाथ जैसी कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफ़ी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद-विचार के विरोधी थे तथा जाति-भेद, वर्ण-भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे।
यहाँ प्रस्तुत पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण-कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित-संपादित कबीर वाङ्मय- खंड 2 (सबद)- से लिया गया है।
पद की संदर्भ व प्रसंग सहित व्याख्या
पद 1. हम तौ एक एक करि जांनां।
दोइ कहैं तिनहीं कौं दोजग जिन नाहिंन पहिचांनां ।।
एकै पवन एक ही पानीं एकै जोति समांनां।
एकै खाक गढ़े सब भांडै एकै कोहरा सांनां ।।
जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटै अगिनि न काटै कोई।
सब घटि अंतरि तँही व्यापक धरै सरूपै सोई।।
माया देखि के जगत लुभांनां काहे रे नर गरबांनां।
निरभै भया कछू नहिं ब्यापै कहै कबीर दिवांनां ।।
संदर्भ― प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक 'आरोह' के काव्य खण्ड के प्रथम पाठ 'पद' - "हम तौ एक एक करि जांनां" से अवतरित है। इसके रचनाकार कबीरदास जी हैं।
प्रसंग― प्रस्तुत पद में कबीरदास ने ईश्वर के एकमात्र स्वरूप के पक्ष में तर्क दिया है और समझाया है कि मनुष्य माया के भँवर में फँसकर घमण्ड न करे।
भावार्थ― कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने यह तथ्य जान लिया है कि ईश्वर एक ही रूप में विद्यमान है। कुछ लोग उस परम सत्ता परमात्मा को जीव-ब्रह्म, आत्मा-परमात्मा आदि दो पृथक् पृथक् अस्तित्व में मानते हैं। वास्तव में ऐसे लोगों ने उस परमात्मा को जाना ही नहीं है। उनके लिए यह संसार नरक के समान है। ऐसे अज्ञानी लोग अपनी अज्ञानता के वशीभूत 'एक में ही दो' स्वरूप देखते हैं। कबीरदास जी ईश्वर के 'एक' होने के पक्ष में तर्क देते हुए आगे कहते हैं कि पूरी सृष्टि में एक ही हवा बहती है, एक ही जल प्रवाहमान रहता है तथा एक ही प्रकाश सभी में समाया हुआ है। कुम्भकार अर्थात कुम्हार भी एक ही मिट्टी को सानकर (गूँथकर) एवं उसे चाक पर चढ़ाकर भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार के बर्तन बनाता है। वे आगे कहते हैं कि जिस प्रकार कोई भी बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है किन्तु उस लकड़ी में छुपी अग्नि का शमन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार मानव का शरीर तो नश्वर (नाशवान) है किन्तु उसमें व्याप्त आत्मा अजर-अमर एवं अकाट्य है। वास्तव में, सभी प्राणियों में एक परमात्मा ही व्याप्त है। उसने ही विभिन्न स्वरूप धारण किए हुए हैं।
कबीरदास जी मानव समाज को चेतावनी देते हुए कहा है कि हे मानव ! पूरा संसार जिस प्रकार मोह-माया के मद में आकर्षित होकर अहंकार में आकण्ठ डूबा हुआ है, वह मिथ्या (झूठा) है। तुझे इस झूठी माया पर गर्व नहीं करना चाहिए। परमात्मा के प्रेम में दीवाना हुए कबीर कहते हैं कि जो लोग मोह-माया के चंगुल से बचे रहते हैं वे निर्भय व निडर रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता।
विशेष (काव्य सौंदर्य)― (1) परमात्मा के एक ही स्वरूप की प्रभावशावी एवं तर्कपूर्ण व्याख्या की गई है।
(2) एक-एक में श्लेष अलंकार है।
(3) 'खाक' और 'कोहरा' में रूपकोतिशयोक्ति अलंकार है।
(4) 'जिन नाहिंन पहिचांनां', 'नर गरबांनां', 'कहै कबीर दिवांनां' में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है।
(5) 'सधुक्कड़ी' भाषा है।
शब्दार्थ (शब्द छवि)
दोजग (फा. दोजख) = नरक
समांनां = व्याप्त
खाक = मिट्टी
कोहरा = कुम्हार, कुंभकार
सांनां = एक साथ मिलाकर
बाढ़ी = बढ़ई
अंतरि = भीतर
सरूपै = स्वरूप
गरबांनां = गर्व करना
निरभै = निर्भय
पाठ का अभ्यास
पद के साथ
प्रश्न 1. कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं?उत्तर - कबीर ने ईश्वर के अद्वैतवादी स्वरूप को स्वीकार करते हुए उसे एक माना है। अपने इस विचार के समर्थन में उन्होंने कई तर्क दिए हैं। उनके अनुसार संसार भर में एक ही हवा चलती है तथा एक ही पानी प्रवाहित होता है। सभी में एक ही प्रकार का प्रकाश विद्यमान है। अर्थात् सारा जगत एक ही परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। वह ईश्वर लकड़ी में अग्नि की तरह समान रूप से व्याप्त है। जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी को सानकर उससे भिन्न-भिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी मूल रूप से एक ही है। कबीर के अनुसार वास्तव में समस्त प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है भले ही प्राणियों के स्वरूप क्यों न भिन्न-भिन्न हों।
प्रश्न 2. मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है?
उत्तर - अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश इत्यादि पाँच तत्वों से मानव शरीर का निर्माण हुआ है।
प्रश्न 3. जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटै अगिनि न काटै कोई।
सब घटि अंतरि तूही व्यापक धरै सरूपै सोई॥
इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है?
उत्तर - उक्त पद की दो पंक्तियों के अनुसार कबीर की दृष्टि में ईश्वर घट-घट में व्याप्त है। लकड़ी के अंदर समायी हुई ऊष्मा (अग्नि) के समान है जिसका शमन बढ़ई नहीं कर सकता। इसी तरह सभी की आत्मा के अंदर उसे ईश्वर का सत्य रूप व्याप्त है।
प्रश्न 4. कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है?
उत्तर - कबीरदास जी ने परमात्मा के सच्चे स्वरूप के साथ साक्षात्कार कर लिया है। उन्होंने मायारूपी जगत तथा स्वयं के अन्दर विद्यमान ईश्वरीय तत्व के मध्य अन्तर को भली-भाँति समझ लिया है। वे बाहरी एवं भौतिक दुनिया के मोह-माया एवं आडम्बरों-पाखण्डों से दूर उस एक स्वरूपा परमात्मा की सच्ची भक्ति में लीन हो चुके हैं। एक साधक के रूप में अपने ईश्वर के प्रति उनकी सच्ची एवं अनन्य भक्ति ने उन्हें पागल सा कर दिया है। सम्भवतः इसलिए कबीर ने अपने को दीवाना कहा है।
पद के आस - पास
प्रश्न 1. अन्य संत कवियों नानक, दादू और रैदास आदि के ईश्वर सम्बन्धी विचारों का संग्रह करें और उन पर एक परिचर्चा करें।
उत्तर― विद्यार्थीगण विद्यालय के पुस्तकालय में से या फिर इंटरनेट के माध्यम से उपर्युक्त संत कवियों के ईश्वर सम्बन्धी विचारों को स्वयं सरलता से संग्रहीत कर सकते हैं। तत्पश्चात् अपने शिक्षकों के कुशल निर्देशन में अपने मित्रों, सहपाठियों के साथ उन विचारों पर चर्चा-परिचर्चा कर सकते हैं।
प्रश्न 2. कबीर के पदों को शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों में लयबद्ध भी किया गया है। जैसे-कुमारगंधर्व, भारती बंधु और प्रह्लाद सिंह टिपाणिया आदि द्वारा गाए गए पद। इनके कैसेट्स अपने पुस्तकालय के लिए मँगवाएँ और पाठ्य-पुस्तक के पदों को भी लयबद्ध करने का प्रयास करें।
उत्तर― विद्यार्थीगण अपने विद्यालय के पुस्तकाल के अध्यक्ष से उपर्युक्त कैसेट्स को मँगवाने के लिए आग्रह करें। साथ ही, वे स्वयं भी इण्टरनेट पर सरलता से कबीर के इन लयबद्ध पदों को डाउनलोड करके उसके आधार पर इस पाठ में संकलित पदों को लयबद्ध करें।
आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
(I hope the above information will be useful and important. )
Thank you.
R. F. Tembhre
(Teacher)
rfhindi.com
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित लिंक्स👇🏻
आरोह भाग 1 (गद्य खण्ड) कक्षा 11 हिन्दी के इन पाठों की अध्ययन हेतु 👇 लिंक्स।
पाठ 1 नमक का दारोगा (मुंशी प्रेमचंद) सम्पूर्ण पाठ एवं पाठ का सारांश एवं संपूर्ण अभ्यास (प्रश्न उत्तर)
इन 👇 प्रकरणों को भी पढ़िये।
1. मूल्य ह्रास क्या है?
2. व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर
3. केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक के कार्य
4. मांग एवं पूर्ति वक्र का एक साथ शिफ्ट होना
5. चेक के प्रकार
इन 👇 प्रकरणों को भी पढ़िये।
1. भारतीय रिजर्व बैंक और इसके कार्य
2. मुद्रास्फीति का अर्थ, परिभाषा एवं महत्वपूर्ण तथ्य
3. अर्थशास्त्र की समझ- आर्थिक गतिविधियाँ, व्यष्टि और समष्टि, अर्थमिति
4. अर्थव्यवस्था एवं इसके प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र
5. आर्थिक प्रणालियाँ- बाजार अर्थव्यवस्था, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था
इन 👇 प्रकरणों को भी पढ़िये।
1. आर्थिक सुधार से संबद्ध- वॉशिंगटन सहमति
2. चीनी आर्थिक विकास का मॉडल- बीजिंग सहमति
3. अर्थव्यवस्था से संबद्ध सैंटियागो सहमति
4. किसी देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जीडीपी एवं इसके प्रयोग
5. एनडीपी से तात्पर्य एवं एनडीपी व जीडीपी में संबंध
6. किसी देश की राष्ट्रीय आय (साइमन कुज्नेट्स के अनुसार)
7. जीएनपी- निजी प्रेषण, विदेशी ऋणों का ब्याज, विदेशी अनुदान
8. एन.एन.पी. की परिभाषा, एन.एन.पी. एवं जी.एन.पी में संबंध
हिन्दी कक्षा 11 के मॉडल प्रश्न पत्र एवं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के इन 👇 प्रकरणों को भी पढ़िये।
1. कक्षा 11 हिन्दी के 50 परीक्षापयोगी वैकल्पिक प्रश्न
2. 50 रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न (उत्तर सहित) हिन्दी कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2025
3. 50 सत्य/असत्य कथन वाले प्रश्न (उत्तर सहित) हिन्दी कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2025
4. पाठ 1 'कबीर के पद (कबीरदास)' 11th हिंदी (आरोह भाग 1 काव्य खंड) पाठ का सारांश एवं अभ्यास
इन 👇 प्रकरणों को भी पढ़िये।
1. कक्षा 11 अंग्रेजी Section C Grammar based Blanks
2. Section C कक्षा 11 अंग्रेजी Grammar based Do as directed (हल सहित)

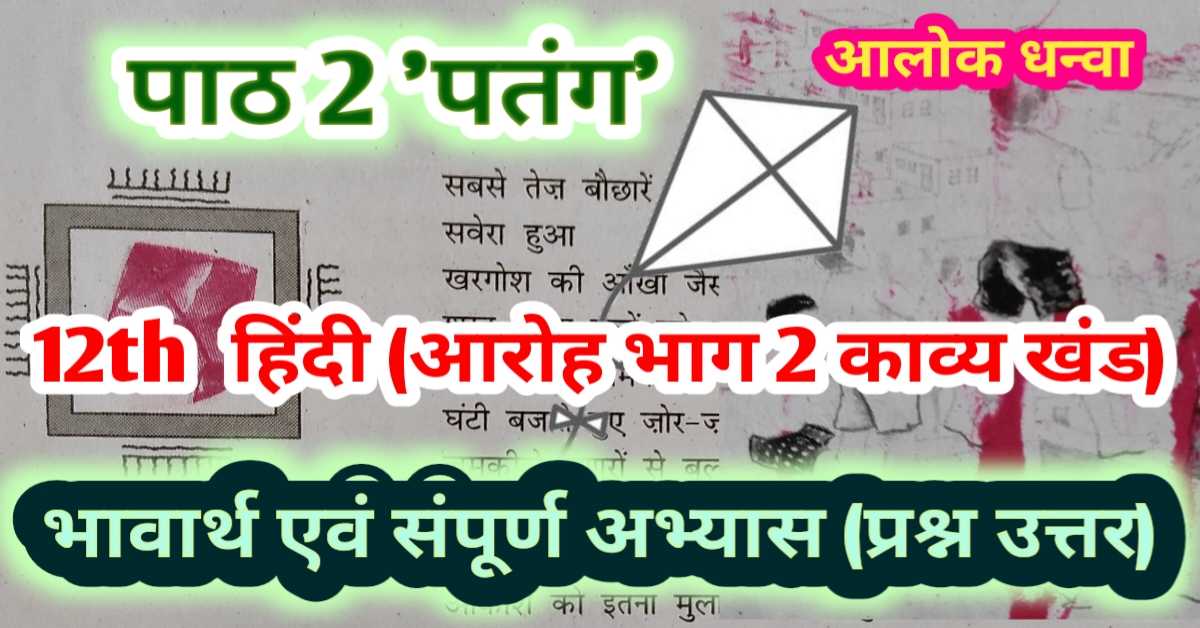
Comments